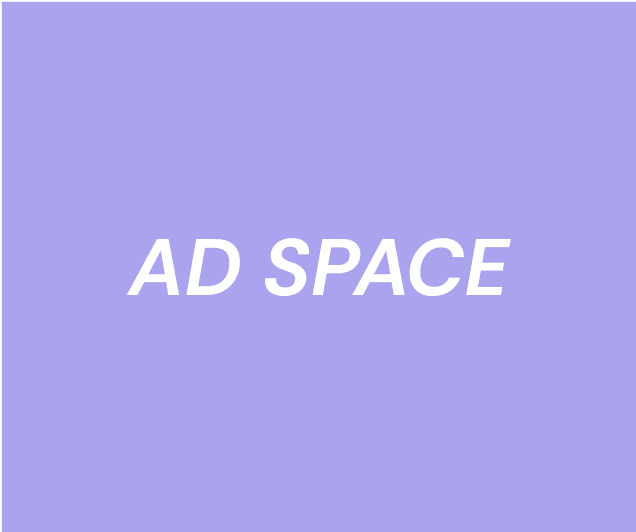“हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अनुकूल माहौल जरूरी है” – रुपेश (माओवादी ज़ोनल प्रभारी)
रिपोर्ट: शैलेश सिंह
(END OF NAXALISM FROM JHARKHAND विषय पर सरकार से मिडिया फेलोशीप अवार्ड प्राप्त)
भारत सरकार ने वर्ष 2026 तक माओवादी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य घोषित किया है। इस सख्त घोषणा के बीच, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उत्तर-पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी “रुपेश” की ओर से 8 अप्रैल को जारी प्रेस बयान ने बहस को नया मोड़ दे दिया है। माओवादी संगठन ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा है कि वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को पहले भरोसेमंद और अनुकूल माहौल बनाना होगा।

सरकार का ऐलान: 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा
केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में संसद में घोषणा करते हुए कहा था कि “देश से वामपंथी उग्रवाद का जड़ से खात्मा वर्ष 2026 तक कर दिया जाएगा।” उनके मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षाबलों की कार्रवाई, विकास परियोजनाओं और सड़क नेटवर्क ने माओवादियों के लिए ज़मीन खोखली कर दी है। गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, 2010 की तुलना में आज माओवादी हिंसा के मामले 70% तक घट चुके हैं।
सरकार का दावा है कि वह “भय मुक्त और निवेश योग्य वातावरण” तैयार कर रही है जिसमें नक्सली गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। साथ ही, प्रभावित राज्यों में बुनियादी ढांचे को मज़बूती से खड़ा किया जा रहा है – सड़कें, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल टावर और रोजगार योजना इसके मुख्य औज़ार हैं।

माओवादियों की प्रतिक्रिया: बातचीत की पेशकश, पर सशर्त
उत्तर-पश्चिम सब जोनल ब्यूरो द्वारा जारी वक्तव्य में माओवादियों ने सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाए हैं। ज़ोनल प्रभारी ‘रुपेश’ ने प्रेस बयान में कहा है:
“हम शांति वार्ता के पक्षधर हैं, लेकिन सरकार पहले हमारे नेताओं की गिरफ्तारी, सैन्य कार्रवाई और गांवों में भय के माहौल को खत्म करे। बिना विश्वास के माहौल के कोई भी वार्ता सार्थक नहीं होगी।”
माओवादी पक्ष ने आरोप लगाया है कि एक ओर सरकार वार्ता का दिखावा करती है, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन समर्थ, ऑपरेशन प्रहार और ग्राउंड डोमिनेशन जैसे अभियानों के ज़रिए आदिवासी जनता को निशाना बनाया जा रहा है।

माओवादी तर्क: “हम विकास विरोधी नहीं, लेकिन विस्थापन के खिलाफ हैं”
माओवादी बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि पार्टी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार का विरोध नहीं करती, लेकिन यह विकास आदिवासियों की “भूमि, जल, जंगल और पहचान” की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
“बिना स्थानीय सहमति के खनन परियोजनाएं, स्टील प्लांट्स और बांध बनाए जा रहे हैं। आदिवासी अपने ही जंगलों में विस्थापित हो रहे हैं। ये युद्ध जैसी स्थितियाँ हैं।” — माओवादी वक्तव्य
उन्होंने सरकार की “विकास की भाषा” को “साम्राज्यवादी और मुनाफाखोर कंपनियों की भाषा” बताया है, जिससे ग्रामीण-आदिवासी समाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

तुलनात्मक विश्लेषण: सरकार बनाम माओवादी – कौन सही, कौन अधूरा?
सरकार का तर्क- माओवादी हिंसा से देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा।
चुनौतियां- जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी, सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध कार्रवाई के आरोप
माओवादी का तर्क- शोषण और विस्थापन के खिलाफ आंदोलन।
चुनौतियां- लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रहना, हिंसा और जन अदालतों का औचित्य
दोनों पक्षों के तर्कों में कुछ यथार्थ हैं तो कुछ विडंबनाएँ भी। माओवादी जहां खुद को आदिवासी हितों का रक्षक बताते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा की गई हिंसा, लेवी वसूली, सरकारी संपत्ति को नुकसान जैसे कृत्य उनकी नैतिकता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।
सरकार के विकास के मॉडल पर भी सवाल उठते रहे हैं – क्या यह सच में समावेशी है, या सिर्फ कंपनियों को सुविधाजनक ज़मीन उपलब्ध कराने का ज़रिया?
स्थानीय आदिवासी जनता: दो पाटों में पिसती ज़िंदगी
शांति वार्ता की प्रक्रिया में सबसे अहम कड़ी है – स्थानीय आदिवासी जनता, जिनके नाम पर दोनों पक्ष लड़ते हैं।
सरकार उन्हें विकास का लाभार्थी बताती है, वहीं माओवादी उन्हें संघर्ष का सेनानी। लेकिन हकीकत यह है कि न तो सरकारी विकास उन तक पूरी तरह पहुँच पाया है, न ही माओवादी संरक्षण ने उन्हें भय और असुरक्षा से मुक्त किया।
झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई गांवों में अब भी स्कूलों को सुरक्षाबलों के कैंप में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी ओर, माओवादियों द्वारा सड़क निर्माण और मोबाइल टावरों का विरोध करना भी स्थानीय लोगों के जीवन में रुकावट पैदा करता है।

पुलिसकर्मियों पर नजरिया: ‘दुश्मन नहीं, समझ के पात्र’
माओवादी वक्तव्य की एक अहम बात यह रही कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को दुश्मन नहीं माना। बयान में कहा गया:
“हमारे विरोध की जड़ व्यवस्था है, न कि कोई व्यक्ति। पुलिसकर्मी भी गरीबों के बेटे हैं। हम उन्हें दुश्मन नहीं मानते।”
यह बयान शांति वार्ता की भावना को मजबूत करता है, लेकिन यह तब ही व्यावहारिक होगा जब मैदान में कार्यरत कैडर और इकाइयाँ इस विचारधारा को अमल में भी लाएँ।
पूर्व प्रयास: वार्ताओं का इतिहास और सबक
भारत सरकार और माओवादी नेतृत्व के बीच इससे पहले भी शांति वार्ता की कोशिशें हुईं, विशेषकर 2004 और 2010 में। लेकिन दोनों ही प्रयास नाकाम रहे।
कभी सरकार ने वादों का पालन नहीं किया तो कभी माओवादियों ने बातचीत के दौरान भी हिंसा नहीं रोकी। परिणामतः “विश्वास की खाई” और बढ़ती गई।

समाधान की राह: क्या संभव है बीच का रास्ता?
शांति वार्ता तब ही सफल हो सकती है जब दोनों पक्ष ‘मध्य मार्ग’ अपनाएं। इसके लिए जरूरी है:
सरकार की ओर से पहल:
सुरक्षा बलों की कार्यशैली में सुधार
विकास योजनाओं में स्थानीय सहभागिता
विश्वास बहाली के प्रतीकात्मक कदम जैसे – गिरफ्तार नेताओं की रिहाई या ऑपरेशन में नरमी
माओवादी पक्ष की जिम्मेदारी:
हिंसा और जबरन वसूली से परहेज
वार्ता को गंभीरता से लेना, न कि रणनीतिक ठहराव
कैडर को प्रशिक्षित करना कि पुलिस और ग्रामीण दुश्मन नहीं
स्वतंत्र मध्यस्थता की व्यवस्था: संवाद के लिए मानवाधिकार संगठन, न्यायविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बीच में लाना
निष्कर्ष: लड़ाई विचारधारा से है, समाधान संवाद से
सरकार और माओवादी दोनों ही अपने-अपने पक्ष में ठोस तर्क रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही तब तक अधूरे हैं जब तक वे आम जनता की ज़मीन पर नहीं उतरते।
हिंसा, चाहे किसी भी पक्ष से हो, अंततः स्थानीय जीवन को ही जख्म देती है। ऐसे में यह जरूरी है कि शांति के लिए न सिर्फ बयान, बल्कि ठोस और भरोसेमंद कदम उठाए जाएँ।